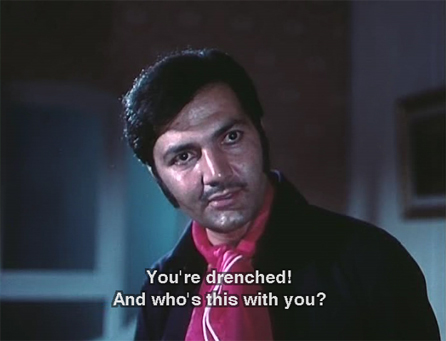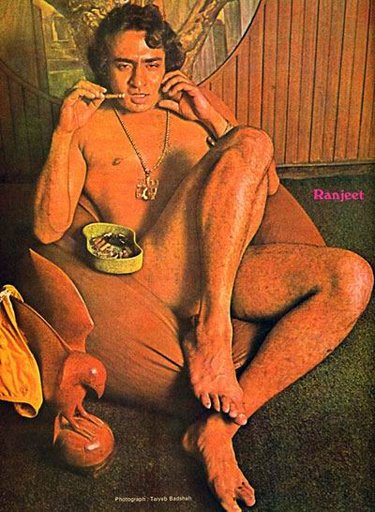If you watched Dangal in theatres, you must have realised the overdose of nationalism. Everyone was forced to stand up for the national anthem not once, but twice. Mihir Pandya‘s essay is on our current state of cinema and nationalism.
If you want to read the same in pdf format, click here.

साल 2014. कुछ बारिश अौर कुछ उमस से भरा अगस्त का महीना, जिसके ठीक मध्य में भारत का स्वतंत्रता दिवस पड़ता है, समाप्ति की अोर था। अचानक दैनिक अखबारों के पिछले पन्नों की सुर्खियों में एक समाचार पढ़ने को मिला। समाचार केरल के तिरुअनंतपुरम से अाया था। समाचार पच्चीस साल के नौजवान लड़के के बारे में था जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (A) के तहत ‘देशद्रोह’ के अारोप में गिरफ़्तार कर लिया गया था।
‘दि हिन्दू’ में प्रकाशित समाचार के अनुसार यह नौजवान अठ्ठारह अगस्त की शाम अपने पांच अन्य दोस्तों के साथ थियेटर में फ़िल्म देखने गया था। उस पर अारोप है कि फ़िल्म शुरु होने से पहले सरकारी तंत्र की अाज्ञानुसार बजनेवाले राष्ट्रगान ‘जन गण मन’, जो एक अन्य समाचार के अनुसार राष्ट्रगान की अधिकृत धुन न होकर दरअसल उसके बोलों पर रचा गया कोई म्यूज़िक वीडियो था[1], की धुन पर वह खड़ा नहीं हुअा अौर इस तरह उसने राष्ट्रगान का अपमान किया। सिनेमाहाल में ही मौजूद कुछ अन्य दर्शकों से नौजवान अौर उसके साथी दोस्तों की इस बाबत बहस भी हुई। इनमें कुछ नौजवान से पूर्व परिचित थे जिन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करवाई। इसमें नौजवान द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले स्वतंत्रता दिवस अौर राष्ट्रध्वज को लेकर की गई कथित टिप्पणी को भी जोड़ा गया अौर बीस अगस्त की रात में पुलिस ने नौजवान को उसके घर से गिरफ़्तार कर लिया।[2]
इस समाचार के बाद भी इस घटना को लेकर छिटपुट खबरें अखबारों में अाती रहीं। छ: सितंबर को प्रकाशित समाचार के अनुसार उनकी ज़मानत याचिका ख़ारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, “उनका कृत्य राष्ट्र विरोधी है और यह अपराध कत्ल से भी ज्यादा गंभीर है।”[3] घटनास्थल पर मौजूद उनके एक साथी ने बताया कि “राष्ट्रगान के वक्त खड़ा होने की हमारी अनिच्छा पर कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर हम खड़े नहीं हो सकते तो पाकिस्तान चले जाएं।”[4]
वेबसाइट ‘काफ़िला’ ने उनका जमानत पर बाहर अाने के बाद दिया गया संक्षिप्त साक्षात्कार प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने कहा था, “मैं अराजकतावादी हूँ… ऐसे व्यक्ति को पैंतीस दिन के लिए ये कहकर जेल में डाला गया कि मैं एक पाकिस्तानी जासूस हूँ। लेकिन मैं एक चीनी जासूस क्यों नहीं हूँ? क्यों मैं सिर्फ़ एक पाकिस्तानी जासूस हूँ? इसकी वजह मेरे धर्म में छिपी है।”[5]
केरल निवासी दर्शनशास्त्र के इस विद्यार्थी का नाम सलमान मोहम्मद है।
2014 के अाज़ाद हिन्दुस्तान में इस घटनाक्रम के बहुअायामी अर्थ हो सकते हैं, अौर होने भी चाहियें। लेकिन मैं यहाँ जिस दिलचस्प तथ्य को रेखाँकित करना चाहता हूँ वो यह है कि इस सारे घटनाक्रम में पक्ष-विपक्ष दोनों अोर से शामिल नागरिक समूह यहाँ अपनी जिस प्राथमिक पहचान के साथ मौजूद है वह लोकप्रिय सिनेमा के दर्शक की पहचान है। ‘राष्ट्रवाद’ की एकायामी विचारधारा पर सवार होकर उपस्थित तमाम ‘अन्य’ पहचानों को ‘राष्ट्रद्रोही’ सिद्ध करनेवाला नागरिक भी यहाँ राष्ट्रगान पर खड़े होने के मूल उद्देश्य से नहीं, सिनेमा देखने के उद्देश्य से पहुँचा है अौर इस ‘राष्ट्रवादी’ के समक्ष खड़ी असुविधाजनक पहचान भी यहाँ उसी सिनेमा के दर्शक के तौर पर मौजूद है।
तिरुअनंतपुरम के किसी अपरिचित सिनेमाघर में किसी अौचक तारीख़ को अपनी पसन्द की फ़िल्म देखने इकट्ठा हुअा यह दर्शक समूह लोकप्रिय हिन्दी सिनेमा, अौर ‘लोकतंत्र’ से उसके जटिल किन्तु गहरे रिश्ते को समझने के लिए कितनी माकूल बुनावट प्रस्तुत करता है। यहाँ सिनेमा भी है, साथ ही यहाँ राष्ट्रवाद भी है। यहाँ उसकी सर्वग्राही परिभाषा भी है तथा साथ ही उस सर्वग्राही परिभाषा को चुनौती की तरह महसूस होती असुविधाजनक पहचान भी है। अौर इन्हें अगर इनकी सिनेमाहाल के मध्य प्राथमिक पहचानों के रूप में पढ़ें तो इनके मध्य लोकप्रिय सिनेमा के दर्शक के बतौर लोकतांत्रिक बराबरी भी है। लेकिन यह ‘कृत्रिम’ बराबरी है, घटनाक्रम अपने गतिशील उद्घाटन में इसे भी बखूबी उजागर करता है।
इस तरह अपनी दर्शकदीर्घा समेत लोकप्रिय हिन्दी सिनेमा का यह ढांचा भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा बोनसायी प्रतीक बन जाता है जिसमें उसकी तमाम खूबियाँ अौर खामियाँ देखी जा सकती हैं। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था उसके व्यावहारिक अौर कार्यकारी पक्ष में जिस प्रकार कार्य करती है, उसे समझने के लिए अचानक लोकप्रिय हिन्दी सिनेमा का ढांचा अकादमिक अौर समाजशास्त्रीय विमर्शों के लिए एक माकूल प्रतीक बन जाता है। यही अाकर्षण नब्बे के दशक की शुरुअात में देश के समाजशास्त्रीय जगत को लोकप्रिय सिनेमा अौर उसकी दर्शक दीर्घा के नज़दीक खींचता है। जैसा समाजशास्त्री अाशिस नंदी रेखांकित करते हैं, लोकप्रिय सिनेमा की तरफ यह अकादमिक मोड़ अस्सी अौर नब्बे के दशक में सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन शैली में अा रहा बदलाव भी परिलक्षित करता है।
नंदी लिखते हैं कि बहुत से विचारक लोकप्रिय हिन्दुस्तानी संस्कृति, खासकर लोकप्रिय सिनेमा की तरफ इसलिए मुड़े क्योंकि यह सांस्कृतिक तथा राजनैतिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। उनकी रुचि मुम्बईया सिनेमा के उद्भव को जानने या व्यावसायिक सिनेमा के इतिहास को जानने में नहीं थी। दरअसल पारंपरिक समाज विज्ञान की तकनीकें, जिनका भारत की परम्परा या स्थानीय परम्पराअों से सीधा कोई लेना देना नहीं था, भारतीय राजनीति में उभरते उन परिवर्तनों को समझने में कोई मदद नहीं कर पा रही थीं। ऐसे में पॉपुलर कल्चर अौर ख़ासकर लोकप्रिय सिनेमा ऐसा महत्वपूर्ण रणक्षेत्र बन गया जहाँ पुराने अौर नए के मध्य, पारंपरिक अौर अाधुनिक के मध्य, वैश्विक अौर स्थानीय के मध्य लड़ाइयाँ मिथक अौर फंतासी में रचा जीवन गढ़कर लड़ी जा रही थीं।[6]
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे भारत के राष्ट्रगान का एकायामी अौर सर्वग्राही किस्म के ‘राष्ट्रवाद’ की स्थापना में इस्तेमाल, अौर वह भी सिनेमा के परदे पर अौर उसकी दर्शकदीर्घा में, यह हालिया दिनों में देखा गया ऐसा अकेला उदाहरण नहीं है। मज़ेदार बात है कि जो दूसरा उदाहरण मैं यहाँ सीधे सिनेमा से उद्धृत करने जा रहा हूँ उसमें भी इस ‘राष्ट्रवादी’ एकायामिता के बरक्स असुविधाजनक पहचानों की उपस्थिति मौजूद है।
अोमंग कुमार द्वारा निर्देशित तथा मुम्बई सिनेमा के चर्चित निर्देशक संजय लीला भंसाली द्वारा निर्मित ‘मैरी कॉम’ उसी दिन चर्चाअों के केन्द्र में अा गई थी जिस दिन इसके पहले पोस्टर सोशल मीडिया में रिलीज़ हुए। इसके अागे अगस्त महीने में फ़िल्म के पहले प्रोमो के सिनेमाघरों में अाने के साथ ही चर्चा, टिप्पणियों अौर अालोचनात्मक लेखों में बदल गई थी। पाँच बार की विश्व चैम्पियन अौर अोलंपिक में पदक जीतने वाली अकेली भारतीय महिला बॉक्सर एम सी मैरी कॉम के जीवन पर बननेवाली इस अधिकृत फ़ीचर फ़िल्म को अचानक विरोधी विचारों की ज़द में लानेवाला तथ्य था फ़िल्म में मणिपुरी बॉक्सर की मुख्य भूमिका निभाने के लिए नायिका प्रियंका चोपड़ा का चयन।
तर्क दिया गया कि इसके पीछे अार्थिक कारण हैं अौर प्रियंका चोपड़ा जैसी स्थापित नायिका के साथ फिल्म को खुले बाज़ार में बेचना अासान होगा। लेकिन अपने अालेख में अभिषेक साहा ने ‘शाहिद’ में राजकुमार यादव अौर ‘गैंग्स अॉफ वासेपुर’ में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी जैसे उभरते अभिनेताअों के चयन के उदाहरण देकर इस तर्क को ख़ारिज किया।[7] ऐसे समय में जब लोकप्रिय हिन्दी सिनेमा चुनौतीपूर्ण मुख्य भूमिकाअों में नए, उभरते कलाकारों को लेकर प्रयोग कर रहा है तब ‘मैरी कॉम’ के निर्माता अौर निर्देशक द्वारा दिया जा रहा बाज़ार का तर्क पूरी तरह गले नहीं उतरता।
जब इंडस्ट्री में उत्तरपूर्व से जुड़ा अौर मूख्य भूमिका कर सकने में सक्षम चेहरा ना मिलने का तर्क दिया गया, समीक्षक असीम छाबड़ा ने अपने अालेख में ऐसे एक नहीं चार चेहरे सामने खड़े कर दिए।[8] एक ऐसे समय में जब भारत के उत्तरपूर्वी हिस्से के नागरिकों के साथ देश की राजधानी में किया जानेवाला भेदभावपूर्ण व्यवहार बहस के केन्द्र में हो, उत्तरपूर्व के छोटे से गांव से निकली इस चावल उगानेवाले किसान की बेटी की भूमिका निभाने के लिए प्रियंका का चयन बहुत अालोचकों को हज़म नहीं हुअा अौर इसे एक ‘खोया हुअा मौका’ कहा गया।
लेकिन मेरा यहाँ इस फ़िल्म का ज़िक्र करने का उद्देश्य इसे लोकप्रिय हिन्दी सिनेमा द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसी प्रतिनिधि फ़िल्म के तौर पर पढ़ना है जिसमें हाशिए की, असुविधाजनक लगती अावाज़ों को सिनेमा अपने भीतर शामिल भी करता है अौर फ़िर इसी क्रम में उनका मुख्यधारा के राष्ट्रवाद के अनुरूप अनुकूलन भी करता है। ‘मैरी कॉम’ की कथा एक ऐसी नायिका की कथा है जिसने अपने जीवन में सामाजिक मान्यताअों को अौर स्त्री अौर पुरुष के लिए वृहत्तर समाज द्वारा निर्धारित की गई तयशुदा भूमिकाअों को हर कदम पर चुनौती दी। अौर इस कथा को सुनाते हुए फ़िल्म भी कुछ दुर्लभ दृश्य परदे पर रचती है। फ़िल्म एक राष्ट्र के तौर पर उत्तरपूर्व के लोगों के साथ अन्य भारतीयों द्वारा किये जाने वाले भेदभाव को प्रतीक रूप में ही सही, परदे पर दिखाती है। एसोसिएशन के अधिकारी, जो अपनी बोली-चेहरे से उत्तर भारतीय लगते हैं अौर जिन्हें अाप भारतीय राष्ट्र-राज्य संस्था के प्रतीक मानकर पढ़ सकते हैं, द्वारा मैरी कॉम को हर कदम पर हतोत्साहित तथा अपमानित किया जाना फ़िल्म में इसका अप्रत्यक्ष प्रतीक मानकर पढ़ा जा सकता है।
लेकिन फ़िल्म का सबसे दुर्लभ हिस्सा वो है जहाँ कथा मैरी की माँ बनने से पहले अौर ठीक बाद की दुविधा को चित्रित करती है। लोकप्रिय हिन्दी सिनेमा ने ऐतिहासिक रूप से ‘माँ’ के किरदार को स्त्री के जीवन की सबसे अादर्श भूमिका बनाकर जिस तरह गौरवान्वित किया है, यहाँ एक स्त्री का ‘माँ’ की भूमिका का निर्धारित अादर्श बनने से अनिच्छा प्रगट करना सिनेमा की ‘मुख्यधारा’ के मध्य एक असुविधाजनक उपस्थिति का होना है।
लेकिन फ़िल्म के अंतिम तीस मिनटों में यह सब कुछ बदल जाता है। फ़िल्म कथा के मध्य में मैरी द्वारा ‘अादर्श माँ’ बनने में दिखाई गई अनिच्छा की जैसे भरपायी करने निकलती है अौर उनके खिलाड़ी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पर उनकी इसी ‘अादर्श माँ’ की भूमिका को अारोपित कर देती है। फ़िल्म के क्लाईमैक्स में उनकी बॉक्सिंग रिंग में गोल्ड मैडल के लिए लड़ाई के ऐन बीचोंबीच उनके नन्हें बेटे के अॉपरेशन के दृश्य पिरोये जाते हैं अौर इस तरह समाज द्वारा तयशुदा ‘माँ’ की भूमिका अपनाने को अनिच्छुक स्त्री की छवि को यह क्लाईमैक्स ‘त्याग की मूर्ति’ किस्म की अादर्श माँ की छवि में अनुकूलित करता है।
इसके ऊपर दोहरा अारोपण होता है राष्ट्रवाद का, जिसमें एक माँ का त्याग ‘राष्ट्र’ के लिए उसके नागरिक द्वारा दी गई कुर्बानी पर अारोपित होकर ‘मदर इंडिया’ की वही क्लासिक छवि गढ़ता है जिसका अाविष्कार लोकप्रिय हिन्दी सिनेमा ने पचास के दशक में बखूबी किया था। अौर इस छवि को पूर्णाहूति देने के लिए यहाँ फिर सिनेमा राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ का प्रतीक रूप में इस्तेमाल करता है।
सुमिता चक्रवर्ती लोकप्रिय हिन्दी सिनेमा पर किए अपने अकादमिक अध्ययन में विस्तार से बताती हैं कि किस तरह पचास के दशक का हिन्दी सिनेमा एक नवस्वतंत्र मुल्क के बाशिंदों को, जिनका सदा से अभ्यास परिवार अौर समाज की सत्ता को सर्वोपरि मानने का रहा है, राष्ट्र-राज्य की संस्था अौर उसके बनाए कानून को अंतिम बाध्यकारी सत्ता मानने का कार्य अंजाम दे रहा है। महबूब ख़ान की ‘मदर इंडिया’ भी इसी क्रम में सामुदायिक जीवन की सर्वोच्च नैतिक संस्था ‘माँ’ पर राज्य की सत्ता का अारोपण कर उसे जनमानस में सर्वोच्च वैधता दिलवाने का काम कर रही थी।
वे लिखती हैं कि पचास के दशक के दर्शक के लिए वो (बिरजू) संभवत: राज्य के कानून द्वारा निर्मित उन सार्वभौम बंधनों को तोड़ने की इच्छा का प्रतीक था जिन्हें शहरी राष्ट्रीय जीवन उन्हें निभाने को बाध्य करता था। यहाँ तक कि यह भी माना जा सकता है कि वो लोगों के मन में उठनेवाली इस तरह की तमन्नाअों से पैदा हुए अपराधबोध का प्राश्चयित करने का मौका भी था। अौर फिर उसे ‘सर्वोच्च सत्ता’ द्वारा सज़ा दिलवाया जाना, जो भारतीय विश्वास में सदा से स्त्री रही है, फ़िल्म का अादिम विश्वासों के माध्यम से नवीन व्यवस्था की स्थापना है।[9]
फ़िल्म के अंतिम दृश्य में जहाँ दुर्गा (नर्गिस) अपने लाड़ले बेटे बिरजू (सुनील दत्त) को अन्तत: गोली मार देती है, यह एक माँ की ममता का − परिवार अौर समुदाय अाधारित प्रेम अौर वफ़ादारी का सर्वोच्च रूप, अाधुनिक राज्य संस्था द्वारा अौर उसके कानून द्वारा अपने नागरिक से मांगी जा रही सर्वोच्च वफ़ादारी के सामने किया तर्पण है। पारिवारिक वफ़ादारियों का, सामुदायिक वफ़ादारियों का, क्षेत्रीय तथा पहचान से जुड़ी वफ़ादारियों का राष्ट्र-राज्य की संस्था के समक्ष नागरिक द्वारा किया तर्पण है।
‘मदर इंडिया’ में नायिका अाधुनिक राज्य अौर उसके कानून के प्रति अपनी वफ़ादारी अपने पुत्र की कुर्बानी देकर साबित करती है, वहीं ‘मैरी कॉम’ की पटकथा में नायिका की इस वफ़ादारी को उसके बच्चे की जान तक़रीबन दाँव पर लगाकर साबित किया गया है। उत्तर पूर्व की महिला बॉक्सर की केन्द्रीय भूमिका वाली यह फ़िल्म पहले हाशिए की अावाज़ों को परदे पर प्रस्तुत करती है अौर फिर खुद ही उन्हें राष्ट्रवाद की चाशनी में अनुकूलित करने का प्रयास भी करती है। यह कोई संयोग नहीं है कि ‘मैरी कॉम’ के निर्देशक अोमंग कुमार ने इसे अपने अौर फ़िल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली नायिका के फ़िल्मी करियर की ‘मदर इंडिया’ का नाम दिया।[10]
‘मदर इंडिया’ की विषयवस्तु अौर प्रस्तुतिकरण को लेकर की गई इस पूरी व्याख्या को हालिया ‘मैरी कॉम’ के समकक्ष रखकर पढ़ें तो पूरी संरचना में असंदिग्ध रूप से समानताएं देखी जा सकती हैं। ‘मदर इंडिया’ जहाँ अपने क्लाईमैक्स में नेहरू की पंचवर्षीय विकास परियोजनाअों से जुड़े प्रतीक − बाँध से निकलते नहर के पानी, को माँ के त्यागमयी अादर्श से जोड़कर राष्ट्र-राज्य का मिथक गढ़ती है, वहीं ‘मैरी कॉम’ अपने क्लाईमैक्स में नायिका के संघर्ष को अौर उसके समूचे व्यक्तित्व को उसके एक ‘माँ’ के रूप में त्याग अौर एक देश के नागरिक की हैसियत से किए त्याग में सीमित करने की कोशिश करती है। साथ ही यहाँ ‘राष्ट्रगान’ का प्रयोग एक खिलाड़ी की विलक्षणता को सिर्फ़ उसके देशभक्ति के जज़्बे तक सीमित कर देखना भी है जो भारतीय सिनेमा खेल पर बनी तक़रीबन हर पिछली फ़िल्म में करता अाया है।
***
लेकिन लोकप्रिय हिन्दी सिनेमा का दर्शक सिर्फ़ वही नहीं देखता जो उसे उसका निर्देशक दिखाना चाहता है। वह उस असुविधाजनक पहचान को भी देखता है जिसका प्रस्तुतिकरण सिनेमा के परदे पर लोकप्रिय सिनेमा क्लाईमैक्स वाले दौर के अनुकूलन से पहले करता है। मैं यहाँ इस तथ्य को जोड़ना चाहूँगा कि लोकप्रिय हिन्दी सिनेमा का दर्शक दुनिया के सबसे ‘सिनेमा साक्षर’ दर्शकों में से एक है। ऐतिहासिक रूप से भी भारत में सिनेमा का विकास प्रथम विश्व के पदचिह्न पर नहीं, उसके तक़रीबन समांतर होता है। 1895 में पेरिस में हुए पहले सिनेमा प्रदर्शन अौर भारत की ज़मीन पर होनेवाले पहले सिनेमा प्रदर्शन में एक साल से भी कम का अंतर है।
जैसा मिहिर बोस अपने इतिहास में लिखते हैं, “सिनेमा के मामले में भारत शुरु से ही इसके वैश्विक विकास की कहानी का हिस्सा रहा तथा टाइपराइटर अौर मोटरगाड़ी जैसे अन्य उन्नीसवीं सदी के अविष्कारों की तरह उन तक पश्चिम के पीछे-पीछे घिसटता हुअा अौर बहुत देर से नहीं पहुँचा। यह दोनों महत्वपूर्ण अविष्कार भी भारत में उसी साल अाकर पहुँचे थे जिस साल सिनेमा का अागमन हुअा लेकिन सिनेमा के उदाहरण से उलट टाइपराइटर का अविष्कार तीस साल पहले ही हो चुका था अौर मोटरगाड़ी भी बम्बई में देखे जाने के दशक भर पहले से यूरोप की सड़कों पर दौड़ रही थी।”[11] भारत के अाम जनमानस का सिनेमा माध्यम से यह अंतरंग परिचय उसके सिनेमा को बरतने की प्रक्रिया को भी सिरे से बदल देता है।
अाम भारतीय शहरी लोकप्रिय सिनेमा को भी वैसे ही बरतता है जैसे वो चुनावी राजनीति को बरतता है। वह उसके द्वारा खड़े किए महावृत्तांत को विभिन्न टुकड़ों में विभक्त कर देता है अौर अपनी छोटी-बड़ी ज़रूरतों के अनुसार अपने काम की चीज़ चुन लेता है। जिस ‘मैरी कॉम’ की संरचना को हिन्दी सिनेमा के लिए एक विषम उपस्थिति − ऐसी स्त्री नायक जो सिनेमा द्वारा रचे ‘माँ’ रूपी भूमिका के तयशुदा अादर्श खाँचे में फिट नहीं होती, को राष्ट्रवाद के वृहत विमर्श में समाहित करने वाली फ़िल्म की तरह पढ़ा जा रहा है, वही फ़िल्म मैरी की तरह एक अौर दर्शकदीर्घा में बैठी जुड़वाँ बच्चों की माँ को यह लिखने का मौका भी प्रदान करती है, “जुड़वां बच्चों की प्रेगनेंसी मेरे लिए कई लिहाज़ से मुश्किल रही थी। जिस वक्त मैं एक अदद-सी नौकरी छोड़ने का मन बना रही थी, उस वक्त मेरे साथ के लोग अपने करियर के सबसे अहम पायदानों पर थे। मैं बेडरेस्ट में थी – करीब-करीब हाउस अरेस्ट में। न्यूज़ चैनल देखना छोड़ चुकी थी क्योंकि टीवी पर आते-जाते जाने-पहचाने चेहरे देखकर दिल डूबने लगता था। किताबें पढ़ना बंद कर चुकी थी क्योंकि लगता था, अब क्या फायदा। यहां से आगे का सफ़र सिर्फ बच्चे पालने, उनकी नाक साफ करने और फिर उनके लिए रोटियां बेलने में जाएगा। गाने सुनती थी तो अब नहीं सोचती थी कि बोल किसने लिखे, और कैसे लिखे। फिल्में देखती थी तो हैरत से नहीं, तटस्थता से देखती थी।
ये स्वीकार करते हुए संकोच हो रहा है कि बच्चों के आने की खुशी पर अपना वक्त से पहले नाकाम हो जाना भारी पड़ गया था। सिज़ेरियन के पहले ऑपरेशन टेबल पर पड़े-पड़े मैं ओटी में बजते एफएम पर एक गाना सुनते हुए सोच रही थी कि मैं अब कभी लिख नहीं पाऊंगी – न गाने, न फिल्में, न कहानियां और न ही कविताएं। दो बच्चों की मां की ज़िन्दगी का रुख़ यूं भी बदल ही जाता होगा न? मेरी कॉम ऑपरेशन थिएटर के टेबल पर डॉक्टर से बेहोशी के आलम में पूछती है, “सिज़ेरियन के बाद मैं बॉक्सिंग कर पाऊंगी न?” वो मेरी कॉम थी – वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर। लेकिन उस मेरी कॉम में मुझे ठीक वही डर दिखाई दिया था जो मुझमें आया था बच्चों को जन्म देते हुए। फिल्म में कई लम्हें ऐसे थे जिन्हें देखते हुए लगा कि इन्हें सीधे-सीधे मेरी ज़िन्दगी से निकालकर पर्दे पर रख दिया गया हो। सिर्फ शक्लें बदल गई थीं, परिवेश बदल गया था, नाम बदल गए थे। लेकिन तजुर्बा वैसा ही था जैसा मैंने जिया था कभी।”[12]
लोक्रप्रिय सिनेमा विरुद्धों का सामंजस्य है। पूंजीवादी समाज व्यवस्था की परियोजना होते हुए भी इसकी सीधी व्यावसायिक निर्भरता इसकी दर्शकदीर्घा पर है। जैसा माधव प्रसाद लिखते हैं, “लोकप्रिय सिनेमा परंपरा और आधुनिकता के मध्य परंपरागत मूल्यों का पक्ष नहीं लेता। इसका एक प्रमुख उद्देश्य परंपरा निर्धारित सामाजिक बंधनों के मध्य एक उपभोक्ता संस्कृति को खपाना है। इस प्रक्रिया में यह कई बार सामाजिक संरचना को बदलने के उस यूटोपियाई विचार का प्रतिनिधित्व करने लगता है जिसका वादा एक आधुनिक- पूँजीवादी राज्य ने किया था।”[13] यहाँ मैं अपनी उस पहले दी गई अवधारणा को दोहराना चाहूँगा जिसे मैं ‘क्लाईमैक्स की भूलभुलैया’ कहता हूँ। मेरा यह मानना है कि लोकप्रिय हिन्दी सिनेमा का क्लाईमैक्स या अन्त जितना यथास्थितिवादी, नैतिकता अौर अादर्श की स्थापना करने वाला अौर असुविधाजनक पहचानों को राष्ट्रवाद की चक्की में समाहित करने वाला है, इसकी कथा संरचना में मौजूद अन्य असंगत लगती पहचानें − जैसे गीत, उपकथाएं, नायकत्व, अतार्किक किस्म का लगता घटनाक्रम अादि सभी समाज की विविधता अौर बहुल पहचानों का अपनी तरह से प्रतिनिधित्व करनेवाली हैं।
यहाँ साल 1998 में प्रकाशित अाशिस नंदी के चर्चित अालेख ‘पॉपुलर सिनेमा एज़ ए सल्म्स अाई व्यू अॉफ़ पॉलिटिक्स’ को भी उद्धृत किया जाना चाहिए जिसने उस दौर में लोकप्रिय सिनेमा के अकादमिक अध्ययन को ठोस वैचारिक ज़मीन देने का काम किया। नंदी लिखते हैं, “लोकप्रिय फ़िल्म के अादर्श उदाहरण में सब कुछ होना चाहिए − शास्त्रीय से लेकर लोक संस्कृति, उदात्त से लेकर हास्यास्पद, अौर अति अाधुनिक से लेकर जड़ हो चुकी परंपराशीलता तक सब कुछ। कथा के भीतर उपकथाएं जो कभी निष्कर्ष तक नहीं पहुँचतीं, मेहमान भूमिकाएं अौर ऐसे स्टीरियोटिपिकल किरदार जिनका पटकथा में कभी पूर्ण विकास नहीं होता। ऐसी फ़िल्में जिनकी कोई निश्चित कथा संरचना नहीं होती अौर जिन्हें एक निश्चित घटनाअों के क्रम द्वारा नहीं समझा जा सकता… एक अौसत ‘सामान्य’ बम्बइया फ़िल्म सबके लिए सबकुछ होने की कोशिश करती है। यह हिन्दुस्तान की अनगिनत जातीयताअों अौर जीवनशैलियों को अपने भीतर शामिल करने का प्रयास करती है अौर विश्वजगत के भारतीय जनमानस पर पड़ते प्रभावों को भी नज़रअन्दाज़ नहीं करती। गैर-प्रबुद्ध किस्म का लोकप्रिय सिनेमा दरअसल अपनी तमाम जटिलताअों, कुतर्कों, भोलेपन अौर क्रूरता के साथ अाधुनिक होता भारत है। लोकप्रिय सिनेमा का अध्ययन भारतीय अाधुनिकता का अपने सबसे अपरिष्कृत रूप में अध्ययन करना है।[14]
यहाँ तक कि जिस नायकत्व की अवधारणा को लोकप्रिय हिन्दी सिनेमा द्वारा यथार्थ को सही-सही हासिल करने की राह में सबसे बड़ी बाधा बताकर पेश किया गया अौर कहा गया कि हिन्दी सिनेमा का नायक परदे पर चाहे कोई भी भूमिका में हो, वह किरदार कम अौर दर्शक का जाना-पहचाना नायक ही लगता है, भी कई बार जटिल भारतीय यथार्थ को समझने में एक अौर परत जोड़ने का काम करती है। शोहिनी घोष सलमान ख़ान के नायकत्व पर अपने अध्ययन में उनकी ‘गर्व’ अौर ‘तुमको ना भूल पायेंगे’ जैसी फिल्मों का विशेष उल्लेख करते हुए बताती हैं कि कैसे हिन्दू किरदार निभाते हुए भी यहाँ सलमान का नायकत्व उस अल्पसंख्यक अाबादी को सीधे संबोधित करता है जिसे नब्बे के दशक के राजनैतिक अौर सामाजिक परिवर्तनों ने अचानक असुरक्षित बना दिया था।[15]
अभिनेता द्वारा किरदार को भेदकर दर्शक से संवाद के इस प्रयोग को एक अौर उदाहरण द्वारा समझें,
राम गोपाल वर्मा की ‘सत्या’ (1998) का सबसे अाईकॉनिक दृश्य वो है जिसमें मनोज बाजपेयी, जो फिल्म में स्थानीय अन्डरवर्ल्ड डॉन भीखू म्हात्रे का किरदार निभा रहा है, मुम्बई के समन्दर के सामने एक ऊँची चट्टान पर खड़ा होकर यह संवाद बोलता है, “मुम्बई का किंग कौन? भीखू म्हात्रे!” असल में यहाँ उसे समन्दर के ‘सामने खड़ा’ कहने के बजाए समन्दर के ‘विरुद्ध खड़ा’ कहना ज़्यादा सही अभिव्यक्ति होगी। वह इस संवाद को किसी चुनौती की तरह अनन्त में उछालता है अौर कमीज़ की बाहों को चढ़ाता हुअा सवाल पूछता है कि क्या इस शहर मुम्बई में कोई है जो उसे चुनौती दे सके। अौर फिर खुद ही जवाब भी देता है, कोई नहीं।
परदे पर इस दृश्य का चाक्षुष गठन कुछ ऐसा है कि इसमें जहाँ भीखू का किरदार दृश्य में सबसे ऊपर नज़र अाता है, मुम्बई की मशहूर ‘स्काईलाइन’ परिदृश्य पर उसके नीचे नज़र अाती है अौर बराबर की तुलनात्मक छवि में दूर क्षितिज पर दिखती बहुमंज़िला इमारतें उसके कद के मुकाबले लम्बाई में छोटी। संवाद के अनुरूप यह दृश्यबंध भी ऐसा परिवेश गढ़ता है जिसमें प्रतीक रूप में मुम्बई शहर भीखू के किरदार के ‘पैरों के नीचे’ नज़र अाता है।
सत्या का यह दृश्य मुम्बई में अाये हर प्रवासी अौर उसकी महत्वाकांक्षाअों का चाक्षुष प्रतीक बन जाता है। प्रवासी, जो सुदूर उत्तर से या धुर दक्षिण से इस शहर में अपना अतीत अौर उससे जुड़े तमाम संबंध छोड़कर अाया है। क्योंकि उसे इस महानगर ने वादा किया था कि यहाँ अपनी मेहनत के बल पर रोज़ी-रोटी कमाने वाले हर इंसान के लिए जगह है। अौर महानगर द्वारा किया यह वादा उस तक पहुँचाने वाला था हिन्दी सिनेमा। सत्या की कथा भी मुम्बई शहर की उसी चिर-परिचित तस्वीर से शुरु होती है जिसका गवाह हिन्दी सिनेमा का इतिहास कई बार रहा है। यह छवि है मुम्बई के मुख्य रेलवे स्टेशन से हाथ में एक अदद बस्ता उठाकर बाहर निकलते नायक की छवि।
पर मज़ेदार बात यह है कि ‘सत्या’ फिल्म का सबसे अाईकॉनिक दृश्य जिस किरदार को देती है, वह फिल्म का घोषित नायक नहीं है। भीखू म्हात्रे यहाँ फिल्म के मुख्य किरदार सत्या के दोस्त की भूमिका में है। अौर इससे भी मज़ेदार बात यह है कि सत्या की तरह वो इस शहर के लिए प्रवासी नहीं है। सत्या के विपरीत उसकी पहचान हमें ज़्यादा अच्छे से मालूम है। फिल्म में उसका घर है, पत्नी है, बच्ची है, अौर उसकी स्पष्टत: मराठी पहचान फिल्म में मौजूद विचार को, अौर खासतौर से इस दृश्य में मौजूद विचार को समझने के लिए जटिल बनाती है। इसे ठीक तरह से समझने के लिए हमें फिल्म के सामान्य कथानक से एक सीढ़ी गहरे जाना होगा।
सत्या जहाँ शहर में प्रवासी नायक का किरदार निभाने के लिए दक्षिण भारतीय अभिनेता चक्रवर्ती को चुनती है, वहीं निर्देशक राम गोपाल वर्मा मराठी गैंगस्टर भीखू म्हात्रे का किरदार निभाने के लिए जिस कलाकार को चुनते हैं वह मनोज बाजपेयी बिहार के बेतिया ज़िले से अाया एक संघर्षशील अभिनेता है। मनोज की ‘सत्या’ से पहले की कहानी में बिहार से अभिनेता बनने का सपना लिए दिल्ली अाने का किस्सा शामिल है तो यहीं दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लगातार दो प्रयास में भी दाखिला ना मिलने की हताशा भी शामिल है। इसके बाद 1993 में दिल्ली से मुम्बई अाकर सिनेमा में अपनी जगह पाने के लिए किया संघर्ष भी शामिल है अौर टिकट कटाकर वापस दिल्ली लौट जाने की निराशा भी शामिल है।[16] इसी बीच उन्हें शेखर कपूर की ‘बैंडिड क्वीन’ में सहायक भूमिका मिलती है अौर यहीं से वे राम गोपाल वर्मा की नज़रों तक पहुँचते हैं।
मुम्बई शहर के सार्वजनिक इतिहास में यही वो समय है जब मुम्बई के राजनैतिक परिदृश्य पर ‘धरतीपुत्र’ बनाम ‘बाहरी’ की राजनीति करनेवाली शिव सेना अपनी रणनीति का प्रमुख निशाना उत्तर भारतीयों, अौर उसमें भी ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश अौर बिहार से अानेवाले गरीब कामकाजी व्यक्ति को बनाने लगती है। नब्बे के दशक में मुम्बई के शिवाजी पार्क में राजनैतिक रैलियों को संबोधित करते हुए शिवसेना नेता बाल ठाकरे एकाधिक बार लिफ्टमैन, चौकीदार, टैक्सी ड्राइवर जैसी तमाम नौकरियों पर एक ख़ास ‘बाहरी समुदाय’ द्वारा होते जा रहे ‘कब्ज़े’ का मुद्दा उठाते हैं अौर इसके पीछे ‘भैय्या’ लोगों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं।[17]
‘सत्या’ में बाजपेयी के किरदार को मुम्बई शहर में खेले जा रहे पहचान की राजनीति के इस नए अध्याय की रौशनी में रखकर पढ़ा जाना चाहिए। जहाँ एक अोर फिल्म सत्या के किरदार के माध्यम से मुम्बई शहर अौर उसके अवैध दायरों में जारी ज़िन्दगी की उठापटक अौर उसमें प्रवासी भारतीय की कथा सुनाने का वादा करती है। वहीं फिल्म के एक मुख्य मराठी पहचान वाले, लेकिन साथ ही सबसे मुखर अौर प्रदर्शनकारी किरदार भीखू म्हात्रे की भूमिका निभाने के लिए उत्तर भारतीय पहचान के मनोज बाजपेयी का चयन करती है। ऐसे में जब दर्शक परदे पर एक मराठी किरदार भीखू म्हात्रे को मुम्बई के अाधुनिक शहरी परिदृश्य की प्रतिनिधि क्षितिजरेखा के समकक्ष, उससे कुछ इंच ऊपर खड़े स्वयं के ‘मुम्बई का किंग’ होने की घोषणा करते देखते हैं तो इसी के समांतर एक उत्तर भारतीय अभिनेता को मुम्बई के समकालीन शहरी परिदृश्य पर बनी एक प्रामाणिक फिल्म में स्वयं को इस प्रदर्शनकारी रूप में अभिव्यक्त करते हुए भी देखते हैं।
यहाँ दर्शक के इस दोहरे अनुभव को इस उदाहरण के माध्यम से समझें। लेखक-निबंधकार अमिताव कुमार मनोज बाजपेयी से जुड़े एक संस्मरण में ‘सत्या’ के इस दृश्य विशेष को देखने के अपने व्यक्तिगत अनुभव को इन शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं, “जिस अभिनेता ने भीखू म्हात्रे का किरदार निभाया था उसका नाम था मनोज बाजपेयी, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था कि उसका जन्म जिस गाँव में हुअा वो चम्पारन बिहार में मेरे गाँव के नज़दीक है। वो स्कूली शिक्षा के लिए बेतिया गया, वो कस्बा जहाँ मैंने भी अपने बचपन के हिस्से बिताये हैं अौर जहाँ अाज भी मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। इसीलिए ‘सत्या’ देखते हुए मैं भीखू म्हात्रे को एक ऐसे भोजपुरी बोलनेवाले व्यक्ति के तौर पर देखता रहा जिसने स्वयं को सिखाकर मराठी वर्चस्व वाले इस महानगर में स्थानीय कहलाने की की परीक्षा पास कर ली है।”[18]
यहाँ नायक की प्रवासी पहचान भी दो हिस्सों में विभक्त हो जाती है अौर जहाँ एक अोर वह सत्या के किरदार की पहचान के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, वहीं दूसरी अोर वह भीखू म्हात्रे के किरदार को निभानेवाले अभिनेता की पहचान से भी अभिव्यक्त होती है। इसीलिए सत्या में अभिव्यक्त मुम्बई में अधिकृत व्यवस्था के सीमांतों पर रहनेवाले निम्नवर्गीय प्रवासी जीवन का जितना चित्रण सत्या के किरदार के माध्यम से मिलता है उतना ही चित्रण भीखू के किरदार के माध्यम से मिलता है।
दरअसल ‘सत्या’ फिल्म में नायक के किरदार को दो हिस्सों में विभक्त कर देती है। सत्या अौर भीखू के किरदारों में। अौर इस तरह भीखू का मुखर किरदार यहाँ शाँत अौर अंतर्मुखी सत्या के लिए उसके ‘अाल्टर इगो’ का कार्य करता है। वह उसका प्रदर्शनकारी द्वय है। भीखू के साथ रहकर सत्या इस शहर में अपनी अभिव्यक्ति पाता है अौर कुछ चरम क्षणों में यह समीकरण इस तरह अभिव्यक्त होता है कि भीखू के प्रदर्शनकारी ‘स्व’ में सत्या का ‘स्व’ अभिव्यक्त होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ दो किरदार मिलकर मुम्बई के परिदृश्य पर एक मुकम्मल प्रवासी पहचान रचने का काम करने लगते हैं। इसकी चरम परिणति यह समन्दर वाला दृश्य है जिसमें सत्या की प्रवासी पहचान अपने सबसे मुकम्मल तौर पर मराठी पहचान वाले मित्र किरदार भीखू म्हात्रे के प्रदर्शनकारी उद्घोष द्वारा अभिव्यक्त होती है।
***
सिनेमा द्वारा किये जाने वाले ‘अनुकूलन’ के अौर विभिन्न पहचानों को प्रतीक रूप में दिखाकर उन्हें वृहत राष्ट्रवाद की कथा में समाहित कर लेने के उदाहरण कई हैं। लेकिन क्या हमारा सिनेमा इसका कोई विलोम भी उपलब्ध करवा पाने में सक्षम है? इस सवाल का जवाब ‘हाँ’ में पाने के लिए भी हमें ठीक उसी तरह लोकप्रिय हिन्दी सिनेमा के दायरे से बाहर निकलना होगा, जिस तरह भारतीय लोकतंत्र की अात्मा को ज़िन्दा रखनेवाली सकारात्मक गतियों को जानने के लिए कई बार हमारा बड़े पैसे अौर बड़ी ताक़त का खेल बन गई चुनावी राजनीति के जंजाल से बाहर निकलना ज़रूरी होता है।
लोकप्रिय हिन्दी सिनेमा के दायरे के बाहर अन्य भाषाअों में बन रहे सिनेमा, वृत्तचित्र सिनेमा, स्वतंत्र फ़ीचर सिनेमा, लघु सिनेमा जैसे तमाम ऐसे विकल्प मौजूद हैं जिनके पीछे बड़े पैसे अौर बड़े प्रदर्शन का वैसा दबाव काम नहीं करता जैसा अाजकल हमारे लोकप्रिय सिनेमा के पीछे हावी हो गया है। हमारे मुल्क में वर्तमान दौर का वृत्तचित्र सिनेमा भारतीय राष्ट्रवाद को चुनौती देनेवाली तमाम हाशिए की अौर असुविधाजनक अावाज़ों का सबसे पसन्दीदा मंच बनकर उभरा है। यह वृत्तचित्र फिल्में ‘सिनेमा के जनतंत्र’ शीर्षक विचार को गज़ब की बहुअायामिता देती हैं। अानंद पटवरधन से लेकर संजय काक तक अौर पारोमिता वोहरा से लेकर बीजू टोप्पो तक वर्तमान दौर में सक्रिय तमाम पीढ़ियों के वृत्तचित्र निर्देशकों की फ़िल्में लोकप्रिय हिन्दी सिनेमा द्वारा अपनी कथा संरचना में मुख्यधारा के अनुरूप किए जा रहे ‘अनुकूलन’ के प्रयासों को चुनौती भी प्रस्तुत करती हैं अौर उनका विकल्प भी उपलब्ध करवाती हैं।
लेकिन यहाँ मैं राष्ट्र की वृहत कथा में अनुकूलन के निरंतर चलते इस सिनेमाई प्रयास को सिरे से उलटने वाली जिस फ़िल्म का ज़िक्र करना चाहता हूँ उसका नाम है ‘फंड्री’। हालिया सालों में मराठी भाषा का सिनेमा जिस तरह समूचे भारत में सबसे उल्लेखनीय फ़िल्में प्रस्तुत करने वाला फ़िल्मोद्योग बनकर उभरा है, उसके उल्लेख के बिना वर्तमान दौर में ‘सिनेमा के जनतंत्र’ की यह कथा पूरी नहीं हो सकती। अौर मज़ेदार बात यह है कि नागराज मंजुले द्वारा निर्देशित यह फ़िल्म भारतीय राष्ट्रवाद अौर राष्ट्र-राज्य की संस्था द्वारा हाशिए की अाबादी से किए वादों अौर उनकी असफलता, उनके ध्वस्त अवशेषों को प्रतीक रूप में दिखाने के लिए क्लाईमैक्स में एक अत्यन्त नाटकीय प्रसंग में उसी राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ का उपयोग करती है जिसका उपयोग ‘मैरी कॉम’ जैसी फ़िल्म में हमने भिन्न पहचानों के ‘अनुकूलन’ की प्रक्रिया में होते देखा।
‘फंड्री’ किशोरवय जाब्या की कथा है जो विलक्षण वाद्य वजाता है अौर जिसे मन ही मन स्कूल में अपनी सहपाठी शालू से प्रेम हो गया है। जाब्या अपने मित्र के साथ मिलकर उस मिथकीय चिड़िया की तलाश में है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे मारकर अगर उसकी राख किसी व्यक्ति पर छिड़क दी जाये तो वह सदा के लिए अापके प्रेम में पड़ जाता है।
यह इक्कीसवीं सदी का हिन्दुस्तान है जहाँ स्कूलों में बाबासाहेब अंबेडकर अौर ज्योतिबा फुले की तस्वीरें दिखाई देती हैं अौर कक्षा में दलित कवि की कविता पढ़ाई जाती है। लेकिन स्पष्ट है कि यहाँ समाज जाब्या अौर उसके परिवार को जाति संरचना में उनकी तयशुदा भूमिकाअों से किसी सूरत में मुक्ति देने को तैयार नहीं। जिस कक्षा में दलित कवि की कविता पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही है, वहीं जाब्या अौर उसके मित्र को पिछले कोने में बाक़ी बच्चों से अलग बैठना पड़ता है। अौर यह व्यवस्था देखकर ऐसा लगता है जैसे इस विरोधाभास को संस्थागत रूप से अपना लिया गया हो। यहाँ दलित अस्मिता को राष्ट्रराज्य के महावृत्तांत में अनुकूलित करने के बजाए ‘फंड्री’ बड़े बारीक स्तर पर इस किस्म के अनुकूलन के पीछे छिपी विडम्बना को हमारे सामने लाती है। ‘फंड्री’ इसे समझने का सबसे बेहतर उदाहरण है कि किस तरह सामंती व्यवस्था से निकली जातिभेद की असमान व्यवस्था का, सबको बराबरी का वादा करनेवाली अाधुनिक राष्ट्र-राज्य संस्था के भीतर ‘अनुकूलन’ हो जाता है।
जाति अाधारित स्तरीकरण में सूअर पकड़ना अौर समूचे गाँव की गंदगी की सफ़ाई जैसे कार्य दलित जातियों के हिस्से कर दिए गए हैं अौर यहाँ प्रदर्शित अाधुनिक समय में जब यह जातियाँ इन कार्यों को छोड़ना चाहती हैं, हम देखते हैं कि समाज की सत्ता व्यवस्था इसे मुमकिन नहीं होने देती। फ़िल्म के अंतिम प्रसंग में, जहाँ जाब्या के ना चाहते हुए भी उसे अपने परिवार के साथ गाँव के अावारा सूअर पकड़ने के काम पर लगा दिया गया है, फ़िल्म न सिर्फ़ समाज की गैरबराबरी दिखाती है बल्कि वो अाधुनिक राष्ट्रराज्य की इस गैरबराबरी को ख़त्म करने में हासिल असफ़लता को भी अपनी ज़द में लेती है।
जाब्या सूअर पकड़ने के इस कार्य से बचना चाहता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि वो यह कार्य करते हुए अपने स्कूल के सहपाठियों की नज़र में अाने से बचना चाहता है। लेकिन अन्तत: उसे अपने बूढ़े होते पिता के दबाव में यह कार्य करना पड़ता है। पिता, जो अब स्वयं यह कार्य छोड़ चुके हैं लेकिन गाँव के सवर्ण सरपंच के अौर बेटी की शादी के लिए पैसा जुटाने के दबाव के चलते कर रहे हैं।
जाब्या अौर उसका परिवार अब उसके स्कूली सहपाठियों के सामने है। उसे अौर उसके परिवार को सूअर पकड़ता देखकर उसके गैर-दलित साथी हँस रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं। यह उनके लिए किसी खेल की तरह है। हँसनेवालों की इस भीड़ में शालू भी शामिल है। जाब्या से यह असहनीय अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा रहा अौर वह चाहता है कि यह जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। लेकिन इसके अन्त के लिए ज़रूरी है उस सूअर का पकड़ में अाना। अन्तत: परिवार मिलकर सूअर को घेर लेता है अौर जाब्या उसे पकड़ने ही वाला है कि तभी − पास में स्कूल की चारदीवारी के भीतर से राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ गाया जाने लगता है। जाब्या अौर उसकी देखादेखी उसका परिवार अपनी जगह स्थिर हो जाते हैं, अौर सूअर अपने रास्ते निकलकर भाग जाता है। इस राष्ट्रगान की सटीक उपस्थिति यहाँ विडम्बना है, अौर यह विडम्बना अाधुनिक राष्ट्र अौर उसके द्वारा अपने नागरिक से एकनिष्ठ राष्ट्रभक्ति के बदले किए गए बराबरी के वादे की कलई खोल देती है।
फ़िल्म सवाल पूछती है कि क्या यह अाधुनिक राष्ट्र-राज्य − जो अपने स्कूलों, अस्पतालों, पुलिस थानों, कचहरियों, संसद भवनों के माध्यम से जनमानस के मध्य प्रगट होता है अौर इन अाधुनिक संस्थाअों के द्वारा अपने नागरिक को बराबरी, न्याय अौर लोकतंत्र का वादा करता है, उस मिथकीय चिड़िया की तरह की कोई संरचना है जिसके बारे में कहा गया कि अगर वो हासिल हो तो अापके मन की हर मुराद पूरी करने में सक्षम है लेकिन असलियत में उसका कोई अस्तित्व नहीं? फ़िल्म बताती है कि भारत जैसे गैर-बराबर मुल्क में अाधुनिक राज्य द्वारा किया समता का यह वादा स्कूल जैसी संस्थागत चारदीवारी से कभी बाहर निकलकर नहीं अाता। अौर अगर कभी उसकी हाशिए पर खड़े अादमी के जीवन में अामद होती भी है तो वह कुछ देने के लिए नहीं, ‘त्याग’ माँगने के लिए। जैसा ‘राउंडटेबल इंडिया’ में फ़िल्म पर लिखते हुए नीलेश कुमार टिप्पणी करते हैं, “अफ़सोस, कि राष्ट्रवाद का यह जुअा हमेशा शोषित तबके के काँधे पर ही जोता जाता है। अौर अगर कहीं वो इसे जोतने से इनकार करे, तो उसे तुरंत ‘राष्ट्रद्रोही’ कहने से नहीं हिचका जाता।”[19]
लेकिन कुछ लोग सिनेमा परदे पर घटता नहीं देखते, वे अपना सिनेमा अपने साथ घर से जेब में रखकर लाते हैं। मैंने यह फ़िल्म मुम्बई फ़िल्म फेस्टिवल में इसकी प्रीमियर स्क्रीनिंग पर देखी थी। निर्देशक ने जान-बूझकर फ़िल्म का विषय, यहाँ तक कि फ़िल्म के नाम ‘फंड्री’ (जिसका अर्थ मराठी दलित समाज द्वारा बोली जाने वाली बोली ‘कैकाड़ी’ में सूअर होता है) का असल अर्थ भी दर्शक से सायास छुपाकर रखा। नतीजा यह था कि प्रतियोगिता में होने की वजह से अौर मराठी सिनेमा की फेस्टिवल सर्कल में हालिया सालों में बनी प्रतिष्ठा के चलते फ़िल्म को खचाखच भरा हॉल तो मिला, लेकिन इसकी दर्शकदीर्घा में फ़िल्म अौर उसके विषय से पूर्वपरिचित चयनित किस्म के दर्शक नहीं थे।
फ़िल्म के अन्त में यह राष्ट्रगान वाला प्रसंग खत्म होने पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा। व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं हतप्रभ था कि कैसे कोई भारतीय फ़िल्म एक साथ जातिवाद को, भारतीय राष्ट्रवाद को अौर इसी राष्ट्रवाद के अनुरूप लोकप्रिय सिनेमा की ‘अनुकूलन’ अाधारित कथा संरचना को एकसाथ चुनौती दे रही है। लेकिन यहाँ भी ताली बजाने की वजहें सबकी एक नहीं थीं। कुछ दूरी पर बैठी मेरी मित्र ने बाद में मुझे बताया कि उनके साथ बैठे बुजुर्गवार राष्ट्रगान की धुन पर जाब्या को सावधान की मुद्रा में खड़ा देख तालियाँ बजाते हुए कह रहे थे, ‘कमाल कर दिया लड़के ने’।
स्पष्ट है कि जिस प्रसंग को हम भारतीय राष्ट्र अौर लोकतांत्रिक व्यवस्था की असफ़लता के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में पढ़ रहे हैं, उसी प्रसंग को कोई अौर राष्ट्रवाद के विजयरथ की जीत के रूप में पढ़ रहा है। यह मेरी नज़र में लोकप्रिय सिनेमा की ‘अनुकूलन’ परियोजना का चरम हासिल है। इसके गवाह खुद ‘फंड्री’ के निर्देशक नागराज मंजुले भी बने। मुम्बई स्क्रीनिंग के बाद जब उनसे दर्शकों की प्रतिक्रिया की बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा, “मैंने हाल ही में यह फ़िल्म लंदन में दिखाई, अौर स्क्रीनिंग में लोगों को हँसता हुअा पाया। मुम्बई में भी तनावपूर्ण दृश्यों में हँसनेवाले बहुत थे।
मेरे ख़्याल से अब हमें यह मान लेना चाहिए कि हम सभी एक ही फ़िल्म अलग-अलग तरह से देखते हैं।… मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि हमारी प्रतिक्रिया इस पर निर्भर होती है कि हम फ़िल्म में किस किरदार से खुद को जोड़ पाते हैं। वे लोग जो जाब्या को चिढ़ानेवाले सहपाठियों से स्वयं को जोड़कर देखते हैं, उन जगहों पर हँसेंगे जहाँ मैं कभी नहीं हँसूंगा। इसके विपरीत जाब्या की करामातों पर हँसनेवाले, जिन्हें मैं हास्य के क्षण मानता हूँ, वस्तुअों को भिन्न दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अौर यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति हँस रहा है लेकिन उसी क्षण वो परेशानी भी महसूस कर रहा है।”[20]
आज लोकप्रिय हिन्दी सिनेमा भले एक ईकाई है, लेकिन उसके जितने दर्शक हैं वो उतनी ही तरह का सिनेमा है।
– मिहिर पांड्या
[6] अाशिस नंदी, पॉपुलर सिनेमा एंड दि कल्चर अॉफ इंडियन पॉलिटिक्स, फिंगरप्रिंटिंग पॉलुलर कल्चर : दि मिथिक एंड दि अाईकॉनिक इन इंडियन सिनेमा, संपादक – विनय लाल अौर अाशिस नंदी, अॉक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2006, पृष्ठ − XXIV
[9] सुमिता एस चक्रवर्ती, नेशनल आईडेंटिटी इन इंडियन पॉपुलर सिनेमा 1947-87, ऑक्सफ़ोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1998, पृष्ठ – 155
[11] मिहिर बोस, बॉलीवुड: ए हिस्ट्री, रोली बुक्स, पेपरबैक संस्करण 2008, पृष्ठ − 39
[13] एम माधव प्रसाद, अाइडियोलॉजी अॉफ दि हिन्दी फिल्म, अॉक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, चौथी अावृत्ति, 2005, पृष्ठ − 113
[14] अाशिस नंदी, इंडियन सिनेमा एज़ ए स्लम्स अाई व्यू अॉफ पालिटिक्स, सीक्रेट पॉलिटिक्स अॉफ अार डिज़ायर्स : इन्नोसेंस, कल्पेबिलिटी एंड इंडियन पॉपुलर सिनेमा, संपादक – अाशिस नंदी, अॉक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1997, पृष्ठ − 7
[15] दि इर्रेज़िस्टेबल बैडनैस अॉफ सलमान ख़ान, शोहिनी घोष, कारावान, अक्टूबर 2012
[16] अनुपमा चोपड़ा, टू अॉफ ए काइंड, इंडिया टुडे, 31 अगस्त, 1998
[17] लायला बावाडाम, डाइवर्सरी टैक्टिक्स, फ्रंटलाइन, 6-19 दिसंबर, 2003
[18] “The actor who played Mhatre was Manoj Bajpai, who I had read was born in a village close to mine in Champaran in Bihar. He had gone to school in Bettiah, a town where I had spent parts of my childhood and where I still have family ties. While watching Satya, therefore, I was watching Bhiku Mhatre as a Bhojpuri-speaking man who had taught himself to pass as a native in the marathi-dominated metropolis.”
− अमिताव कुमार, राइटिंग माई अोन सत्या, दि पॉपकॉर्न ऐस्सेइस्ट : व्हाट मूवीज़ डू टू राइटर्स, संपादक – जय अर्जुन सिंह, ट्रांक्युबार, नई दिल्ली, 2011, पृष्ठ − 78-9
It was originally written for ‘Aalochana’ (edited by Apoorvanand) in 2014.